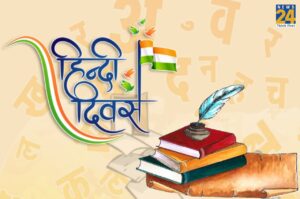

वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रवाल
प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। क्या यह दिवस सिर्फ बधाई, शुभकामनाएं लेने- देने की औपचारिकता तक ही सीमित रहेगा। या फिर छोटे- बड़े कुछ सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर ही हिन्दी के प्रति हमारे कर्तव्य की इतिश्री कर ली जायेगी। पत्रकारिता जगत में मेरे एक सहकर्मी मजाकिया अंदाज में कहा करते थे- आ गया सितम्बर महीना। अब मनाया जायेगा हिन्दी पकौड़ा (वे पखवाडा को पकौड़ा कहा करते थे)। कुछ लोग पकायेंगे, कुछ खायेंगे, कुछ सुगंध से ही संतुष्ट होंगे। हमें (उन पत्रकार महोदय को ) भी कुछ सरकारी कार्यक्रमों में बुलाकर अतिथि, जज (विभिन्न तरह की प्रतियोगिता के लिए ) बनाया जायेगा, दिव्य नाश्ता मिलेगा, कुछ पाकेट खर्च भी। बस और क्या। औपचारिकता पूरी। उपर के सरकारी आदेश की खानापूर्ति। इसके लिए आवंटित बजट का एन केन प्रकारेण स्वाहा। पर पखवाडा मनाने की मूल भावना यानि हिन्दी की सर्वांगीण उन्नति से इन आयोजनों का कोई लेना-देना नहीं। हालांकि मेरे मित्र मजाक में प्रति वर्ष अपना पकौड़े वाला जुमला दोहराते थे, पर एक अंश तक यह कड़वी सच्चाई है।
हमने हिन्दी को राजभाषा तो बनाया, इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिला, पर वास्तविक अर्थो में पूरे देश में इसे लागू नहीं करा पाये। राजनीति के दलदल में यह मामला ऐसा फंस गया है कि अहिन्दीभाषी राज्यों में राजकाज की भाषा में हिन्दी को वरीयता देने के किसी भी कदम का जोरदार विरोध किया जाता है। यहां मजे की बात यह है कि उन राज्यों की आंचलिक भाषा को पहली वरीयता के बाद हिन्दी को स्थान देने की बात भी उनके गले नहीं उतरती। हम अंग्रेजों के शासन से तो मुक्त हुए पर अंग्रेजी की मानसिक से नहीं। इन राज्यों के मूल निवासियों को लगता है कि हिन्दी उन पर थोपी जा रही है। वोट की राजनीति तो इस भावना को भड़काने में कोढ़ में खाज का काम करती है। क्या इस परिस्थिति के लिए इन राज्यों के मूल निवासी दोषी हैं। जी नहीं, उनसे ज्यादा दोषी हम हिन्दी भाषी हैं। केन्द्र या राज्यों में बैठे वे राजनीतिज्ञ व अफसरशाही जिम्मेवार है, जिन पर हिन्दी भाषा को हर तरह से सक्षम बनाने का गुरुतर भार है। दरअसल इस मसले की जड़ में रोजी- रोटी की व्यवस्था है, वह चाहे नौकरी हो या व्यवसाय। हम अदालतों मे काम काज, विज्ञान की उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए पुस्तकें, कम्प्यूटर में सुचारू रूप से काम करने के लिए हिन्दी में उच्च तकनीक का विकास जैसे काम तीव्र गति से नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा पीछे जाय तो आजादी के बाद केन्द्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों विशेषकर जवाहरलाल नेहरू की भाषा नीति की गलतियों का खामियाजा हम आज तक भुगतान रहे हैं। वोट की तुच्छ राजनीति व कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने इस मसले को ऐसी गलत दिशा में मोड़ दिया कि हिन्दी व अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के बीच इस समय सगी बहनों का रिश्ता न होकर ऐसी सौतन का रिश्ता बन गया जो बिना किसी समुचित कारण के किसी भी छोटी सी बात पर लड़ने- झगड़ने को तैयार रहती हैं। और इस माहौल का फायदा उठा रही है अंग्रेजी भाषा, जो अपने किसी आका के परिश्रम के ही हमारे सिर का ताज बनी हुई है। आज हमारे अधिकांश नौजवानों में यह भावना मजबूत होती जा रही है कि बिना अंग्रेजी ज्ञान के न हम अपने देश में और ना ही विदेश में अच्छा रोजगार पा सकते हैं।
आज के माहौल में भले हमें यह भावना सटीक लगती हो, परन्तु यह बात एकदम सही नही है। अभी भी यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति व संकल्प का परिचय दे तो बहुत कुछ हो सकता है। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। कई दशकों पुरानी बात है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शांता कुमार ने कोलकाता में एक मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प घटना बतायी थी। उन्होंने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो राजकाज का काम पूर्णतया हिन्दी में करने के लिए क्या करना होगा, यह अफसरों से पूछा। अफसरों ने बताया कि सबसे पहले टाइपराइटरों को उस लायक बनाना होगा। (ज्ञातव्य है कि उन दिनों हर काम में टाइपराइटरों की ही प्रमुखता थी, जो सिर्फ अंग्रेजी में ही टाइप किया करते थे )। श्री कुमार ने आगे बताया- मैंने पूछा कि हिन्दी में काम करने के लिए टाइपराइटरों को बदलने में कितना समय लगेगा, तो उनलोगों ने एक लम्बा समय बता दिया। साथ ही लम्बा- चौड़ा खर्च व काफी दिक्कतें आयेंगी, ऐसा बताया। दरअसल वे (अफसर) चाहते ही ही नहीं थे कि यह बदलाव आये, कयोंकि उन्हे नये सिरे से प्रशिक्षण लेना पड़ता। शांता कुमार जी ने बताया- मैंने इस बारे में पहले ही जानकारी ले ली थी कि कितने समय और खर्च में यह काम हो जायेगा। अत: अफसरों से साफ- साफ कहा- इतने दिनों के अन्दर यह काम हो जाना चाहिए, अन्यथा नतीजे भुगतने को तैयार रहें। आश्चर्यजनक रूप से वह काम निर्धारित समय से पहले ही हो गया। कहने का अर्थ यह है कि यदि प्रशासक इमानदारी व दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कुछ करने की ठान ले तो निश्चित रूप से बदलाव ला सकता है।
ऐसा नहीं है कि हिन्दी में क्षमता नहीं है या फिर वह लोकप्रिय नहीं है। अब तो विदेशों में भी यह भाषा काफी प्रचलित हो रही है और विदेशी छात्र- छात्राएँ इसे सीख रहे हैं। 44 वर्ष पहले 1980 में जब प्रिंस चार्ल्स (जो अब ब्रिटेन के महाराजा बने चुके हैं ) कोलकाता आये थे, तब साहागंज स्थित डनलप फैक्टरी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुझसे हिन्दी के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखायी थी और मैंने कुछ शब्द उन्हे सिखाये थे। इस बारे में मीडिया मे रिपोर्टें भी छप चुकी हैं। भले ही हिन्दी अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा नहीं बनी हो, पर तेजी से जन- जन की भाषा बनती जा रही है। उल्लेखनीय है कि आजादी के पहले कई देशभक्त अहिन्दीभाषी विद्वानों ने हिन्दी के प्रचार- प्रसार में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस समय हिन्दी फिल्में, गाने, कविताएं अहिन्दीभाषियों में विशेषकर युवाओं में लोकप्रिय हो रही हैं, जो प्रकारान्तर से हिन्दी के प्रचार- प्रसार में सहायक है। यदि हम इस भावना में बदलाव ला सके कि हिन्दी का विकास किसी अन्य भारतीय भाषाओं के लिए घातक नहीं बल्कि उसकी उन्नति में सहायक है तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। साथ ही केन्द्र को यह भी बताना होगा कि हिन्दी किसी भी गैर हिन्दीभाषी राज्य पर थोपी नहीं जायेगी। साथ ही यह समझाया जाना चाहिए कि देश के सभी राज्यों के बीच सही अर्थों मे समन्वय के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में इसका प्रचलन कितना उपयोगी है। देश की एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखने व मजबूत बनाने में ऐसा करना कितना आवश्यक है। अगर समय रहते हम यह काम कर पाये और आम जनता को यह दिखा पाये कि अकेले हिन्दी के अच्छे ज्ञान के बलबूते पर आप न सिर्फ देश के किसी भी भाग में बल्कि विदेशों में भी पूरे सम्मान के साथ आजीविका चला सकते हैं तो हिन्दी अपने आप सिरमौर बन जायेगी।
(लेखक प. बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जो पांच दशक से इस क्षेत्र में हैं )

